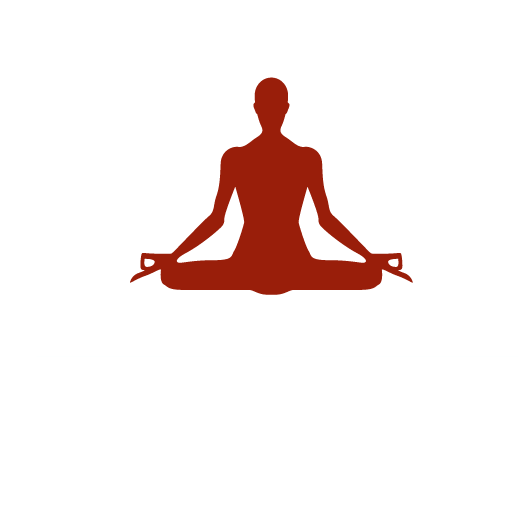दर्शन: मानसिक स्वास्थ्य का आधार
11 months ago By Yogi Anoopदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य: रोगों के निदान में इसकी भूमिका
दर्शन: मानसिक स्वास्थ्य का आधार
दर्शन का अर्थ केवल बाह्य रूप से देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दृष्टा (आत्मा) के अपने अस्तित्व को अनुभव करने की प्रक्रिया है। जब दृष्टा, दृश्य को देखने तक सीमित रहता है, और दृश्य से ही आत्मसंतोष प्राप्त करने की ही चाहत रखता है, तब तक उसे आत्मबोध नहीं हो पाता है। वह इसलिए कि दृष्टा, दृश्य के सीमित दायरे से पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता है। दृश्य स्वयं में सीमित है, इसलिए दृष्टा को पूर्ण संतोष नहीं दे सकता है। यही असंतोष दृष्टा में असंतोष पैदा करके भटकाता है और अंततः दैहिक रोग को जन्म देने का कार्य करता है।
किंतु भारतीय दर्शन में ‘दर्शन’ शब्द का अर्थ दृश्य के दर्शन से नहीं, बल्कि दृश्य को छोड़कर दृष्टा स्वयं के दर्शन से है। अर्थात् दृष्टा, दृश्य को न अनुभव करके स्वयं का दर्शन कर ले, तो वह वास्तविक दर्शन कहलाता है। यही दर्शन उसके जीवन की सभी शंकाओं को दूर कर देता है तथा साथ-साथ उसको स्वयं में ही स्थिर चित्त करवा देता है। चित्त की यही स्थिरता से देह-मस्तिष्क स्वयं को स्वयं के द्वारा सर्वाधिक हील करता है।
मेरे प्रयोगों में आध्यात्मिक रोगों का जन्म तभी संभव होता है जब स्वयं के दर्शन…
मानसिक रोगों का मूल कारण यही है कि व्यक्ति बाहरी संसार में इतना लीन हो जाता है कि वह स्वयं को भूल जाता है। उसका मन बाह्य वस्तुओं में उलझ जाता है और इस उलझाव के कारण मन, मस्तिष्क और शरीर असंतुलित हो जाते हैं। यदि व्यक्ति दर्शन के सही अर्थ को समझ ले, तो वह स्वयं को इन मानसिक रोगों से मुक्त कर सकता है।
‘दर्शन’ और मानसिक रोगों का संबंध
दृष्टा का दृश्य तक ही सीमित रहना बुद्धि के विकास को सीमित कर देना है। मेरे अनुभव में बौद्धिक क्षमता जितनी सीमित होती जाती है, उतना ही सोचने का दृष्टिकोण भी सीमित होता जाता है। और ध्यान दें, सीमित दृश्यों से मानसिक तनाव को रोका नहीं जा सकता है। अर्थात् सीमित दृष्टिकोण से किसी भी समस्या के समाधान को अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता है।
एक और तथ्य यहाँ पर समझना चाहिए कि सीमित दृश्यों से जीवन को अच्छी तरह से जीना संभव नहीं हो सकता है।
• यदि सीमित दृष्टिकोण से दृष्टा स्वयं को दृश्यों में उलझा लेता है, उसे ऐसा भ्रम होता है कि वह दृश्यों में रहकर पूर्ण संतुष्ट हो जाएगा, किंतु यह संभव नहीं हो पाता है। अंततः परिणाम में उसे तनाव, चिंता और अवसाद का शिकार होना ही पड़ता है।
• जब दृष्टा, दृश्य के सीमित दायरे में ही स्वयं के जीवन का पूर्ण आधार मानता है, तब उसके चित्त में स्थिरता का उन्मूलन हो जाता है। यही उसके चित्त में वृत्ति को कम नहीं होने देता है। अर्थात् परिणाम में दुख, कष्ट और रोग ही मिलते हैं।
• मानसिक अस्वास्थ्य का प्रथम सूत्र दृष्टा द्वारा दृश्य में भावनाओं को इतना पैदा करना है कि उसी में उलझ जाना और उससे स्वयं को बाहर न निकाल पाना। संभवतः इसीलिए पतंजलि योगसूत्र में दृष्टा का दृश्य से अलगाव होना पूर्ण स्थिरता बताया गया है और साथ-साथ वृत्ति के पूर्ण निरोध में आत्मबोध अर्थात् स्वयं के स्वरूप का बोध हो जाता है। जो दृष्टा के स्वरूप का ही लक्षण होता है। यही स्वयं में स्थित होने का पूर्ण लक्षण है।
स्वरूप दर्शन (आत्मदर्शन) से मानसिक रोगों का समाधान
चित्त की वृत्ति के पूर्ण निरोध अर्थात् दृष्टा, दृश्य का निरोध कर देता है, तब “तदा दृष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्” अर्थात् स्वरूप का दर्शन हो जाता है। स्वयं के स्वरूप का दर्शन व अनुभूति से संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था में किसी भी प्रकार के मानसिक दोष के लक्षण नहीं दिखते हैं। यहाँ तक कि वह किसी भी प्रकार की वैचारिक लतों से स्वयं को मुक्त करवा लेता है।
• आत्मानुभूति, स्वयं को सभी मानसिक भ्रमों से परे कर देती है। भ्रम से परे की यही अनुभूति मानसिक स्थिरता देती है, जो मस्तिष्क और देह में सेरोटोनिन नामक रसायन को संतुलित करने में सहायक भी होती है। ध्यान दें, यही स्थिरता भावनाओं से तटस्थ करती है। यही संतोष भी पैदा कर देती है। यह संतोष कभी न मिटने वाला होता है। इसीलिए इस प्रकार के व्यक्तित्व में रसायनों और हार्मोन्स में असंतुलन होने की संभावनाएँ नहीं रहती हैं।
• यह भी ध्यान दें, जब सेरोटोनिन जैसे रसायन का प्रभाव अधिक बढ़ता है, तब तनाव वाले हार्मोन (कॉर्टिसोल) में स्वाभाविक रूप से कमी आने लगती है।
‘दर्शन’ और अच्छी नींद का संबंध
स्वयं के स्वरूप की अनुभूति इतनी गहरी होती है कि उस अनुभूति में दृश्य का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। यही दृष्टा की स्थिरता का मूल आधार है और स्थिरता ही उसकी निद्रा में अत्यंत सहयोग करती है। वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए, तो सेरोटोनिन जैसा रसायन मेलाटोनिन की वृद्धि में सहायक होता है। मेलाटोनिन रसायन ही निद्रा के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है।
इसीलिए मैं उन सभी लोगों से असहमत हूँ, जो नींद को लाने के लिए थकने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे अनुसार, नींद का संबंध शारीरिक थकान मात्र से नहीं, बल्कि मानसिक शांति से है। जब दृष्टा, दृश्य से स्वयं को मुक्त करवाता है, तब उसमें मानसिक उलझनें समाप्त हो जाती हैं और उसमें निद्रा से संबंधित आशाओं का समाधान हो जाता है।
मैं अनुभवपूर्वक कहता हूँ कि गहन निद्रा का अर्थ है मानसिक उलझनों से स्वयं को परे करवा लेना। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से गहन निद्रा भयानक से भयानक मानसिक रोगों के निराकरण का प्रमुख माध्यम है। ज्यादातर मानसिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति में निद्रा का अभाव दिखने लगता है। जैसे-जैसे दृष्टा, दृश्य से स्वयं को मुक्त करवाने लगता है, वैसे-वैसे मानसिक विश्राम गहराई से प्राप्त होने लगता है और अनिद्रा जैसी समस्याएँ समाप्त होने लगती हैं।
• दृष्टा का दृश्य से अलगाव होने का अर्थ ही है मानसिक विश्राम, और मानसिक विश्राम का अर्थ है मेलाटोनिन की मात्रा का अत्यधिक होना। और मेलाटोनिन की वृद्धि होने का अर्थ है संपूर्ण देह का स्वयं के द्वारा स्वयं से हीलिंग होना।
• स्थिरता, जो कि गहन निद्रा देती है, से तंत्रिका तंत्र स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है, जिससे इच्छाशक्ति ही नहीं, बल्कि देह में होने वाले कई समस्याएँ साथ ही समाप्त होने लगती हैं।
भारत में कई दार्शनिक मत हुए हैं, जो कहीं न कहीं सभी का मत दृष्टा का दृश्य से मुक्ति ही है। इसलिए मेरे मत में किसी भी दार्शनिक व्याख्याओं का अभ्यास किया जा सकता है। किंतु मेरे अपने अभ्यास में सांख्य और पतंजलि दर्शन स्वयं में एक परिपूर्ण दर्शन है, जो जीवन के मूल रहस्यों को समझाकर स्वयं को स्वयं में स्थित करवा देता है। यही आत्मदर्शन है, यही मोक्ष है। इसमें ध्यान, योग, प्राणायाम, आसन इत्यादि साधन हैं, जो अत्यंत ही उपयोगी होते हैं।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy