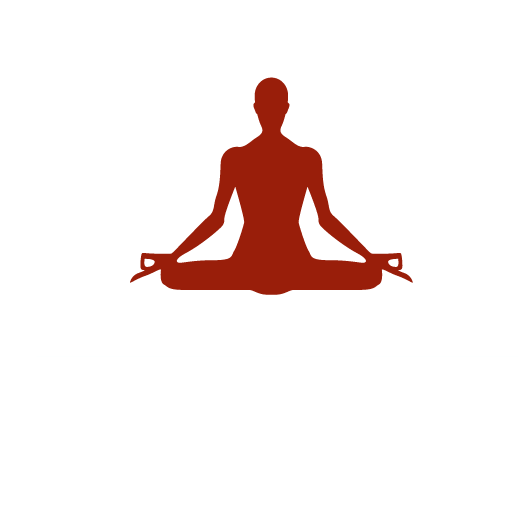“मैं क्या हूँ?” — नेति से एतत् की ओर ध्यान की यात्रा
1 week ago By Yogi Anoop“मैं क्या हूँ?” — नेति से एतत् की ओर ध्यान की यात्रा
उपनिषदों में एक मार्ग है — नेति नेति। इसका अर्थ है — “यह नहीं, यह नहीं”। यह आत्मा की खोज में एक प्राचीन पद्धति है, जिसमें साधक यह समझ और अनुभव विकसित करने का प्रयत्न करता है कि वह न तो शरीर है, न प्राण है, न मन, न बुद्धि; न यह जगत है, न उसमें व्याप्त किसी भी वस्तु का अंश। अर्थात् वह प्रकृति नहीं है । यद्यपि यह एक प्रकार का निषेध है, जिससे पुरुष व “मैं” प्रकृति को बार बार यह कहता है कि मैं तुम नहीं हूँ ।
किन्तु यह पथ कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, यह एक सीमा के बाद एक अंतहीन निषेध करते रहने का भ्रम भी रच सकता है — जैसे कोई बार-बार यह कहे कि मैं यह नहीं हूँ, वह नहीं हूँ, तो कुछ वर्षों के अभ्यास के बाद स्मृति में “मैं यह नहीं हूँ” ही प्राथमिकता से चलने लगता है और लगता है कि जीवन का उद्देश्य ही यह है ।
यह सत्य है कि साधना के प्रारंभ में व्यवहारिक समझ को विकसित करने के लिए “मैं” को अपने करीबी देह और इन्द्रियों के साथ व्यावहारिक अनुभव करना पड़ता है कि मैं यही देह नहीं हूँ , मैं इन्द्रियाँ नहीं हूँ बाद में यह सिद्ध होता है मैं विषय व प्रकृति नहीं हूँ । इससे अलगाव की अनुभूति होती है । उन लोगों के लिए यह अनुभूति बहुत आवश्यक है जो मानसिक रूप से वस्तुओं , देह और इन्द्रियों , कल्पनाओं से इतना चिपके हैं कि मानसिक विकार उत्पन्न हो चुके हैं । अंततः विषय से स्वयं के अलगाव की अनुभूति के लिए यह अभ्यास उत्तम है किंतु वह भी प्रारंभिक साधना में । यह तरीका उन लोगों पर भी कार्य करता है जो थोड़ा सा नकारात्मकता में अधिक जुड़े हुए होते हैं । विषयों में अधिक लिप्त होते हैं । इसीलिए विषयों को समझने के लिए नेति नेति के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है ।
किंतु पुरुष का मूल उद्देश्य यह ज्ञात करना नहीं कि वह क्या नहीं है, मूल उद्देश्य तो यह ज्ञात और अनुभव करना है कि वह क्या और कौन है । उसे उन तत्वों के बारे में जानकारी कर लेने से प्रसन्नता अवश्य होती है कि वह क्या नहीं किंतु उससे वह पूर्ण संसयरहित, पूर्ण शांत पप्रसन्न और आत्मबोध अवस्था में नहीं आ सकता है ।
इसीलिए मैं हमेशा से इस साधना का पक्षधर रहा हूँ कि ध्यान की यात्रा अपने असली में स्वयं के ज्ञान के लिए ही शुरू होती है। इसीलिए ध्यान कोई बौद्धिक निषेध नहीं है — यह तो प्रत्यक्ष अनुभूति है। ध्यान में जब “मैं” की अनुभूति सघन होती है, तो उस क्षण यह जानना ज़रूरी नहीं रह जाता कि “मैं क्या नहीं हूँ” — क्योंकि उसी क्षण प्रत्यक्ष और व्यावहारिक रूप से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भी “मैं” क्या क्या नहीं नहीं हूँ । इसका ज्ञान स्वतः ही होना चाहिए ।
नेति-नेति कहते रहना व नेति नेति का प्रत्यक्ष अनुभव करने से भी आत्मा की उपलब्धि में बाधाएं आ सकती हैं । इसके विपरीत यदि साधना में “एतत् अस्ति — यह है, यह है” का भाव, एक मौन उद्घोष की तरह भीतर जागता है — और वह उद्घोष यही है: “अहमस्मि” — मैं हूँ।
एक बालक को देखिए — वह यह नहीं कहता कि “मैं जल नहीं हूँ, मैं वायु नहीं हूँ, मैं यह ब्रह्मांड नहीं हूँ।” वह सहज रूप से बस ‘मैं’ होता है । यह उपस्थिति ही उसकी सबसे बड़ी घोषणा है। इसी तरह ध्यान की गहराई में उतरने पर आत्मा स्वयं को प्रमाणित करती है — किसी तर्क या निषेध से नहीं, बल्कि अपने “होने” से।
उपनिषदों में यह भी आता है:
“प्रज्ञाने ब्रह्म”— ब्रह्म ही चेतना है। और जब यह चेतना अपने आप में टिकी होती है, तब न उसे यह कहने की आवश्यकता रहती है कि वह क्या नहीं है, और न ही यह सिद्ध करने की कि वह क्या है। उस क्षण “मैं हूँ” — यही उसकी पूर्णता है।
इसलिए ध्यान की साधना में निरंतर यह विचार व अनुभव करने के बजाय कि “मैं क्या नहीं हूँ”, साधक को यह मौन भाव जागृत करना होता है कि — “मैं हूँ — और यह होना ही परम सत्य है।”
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy