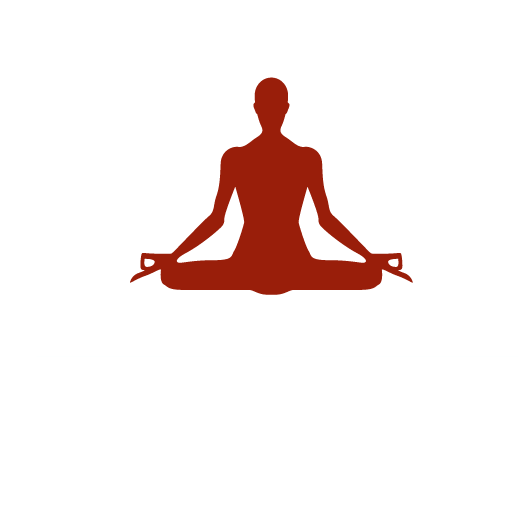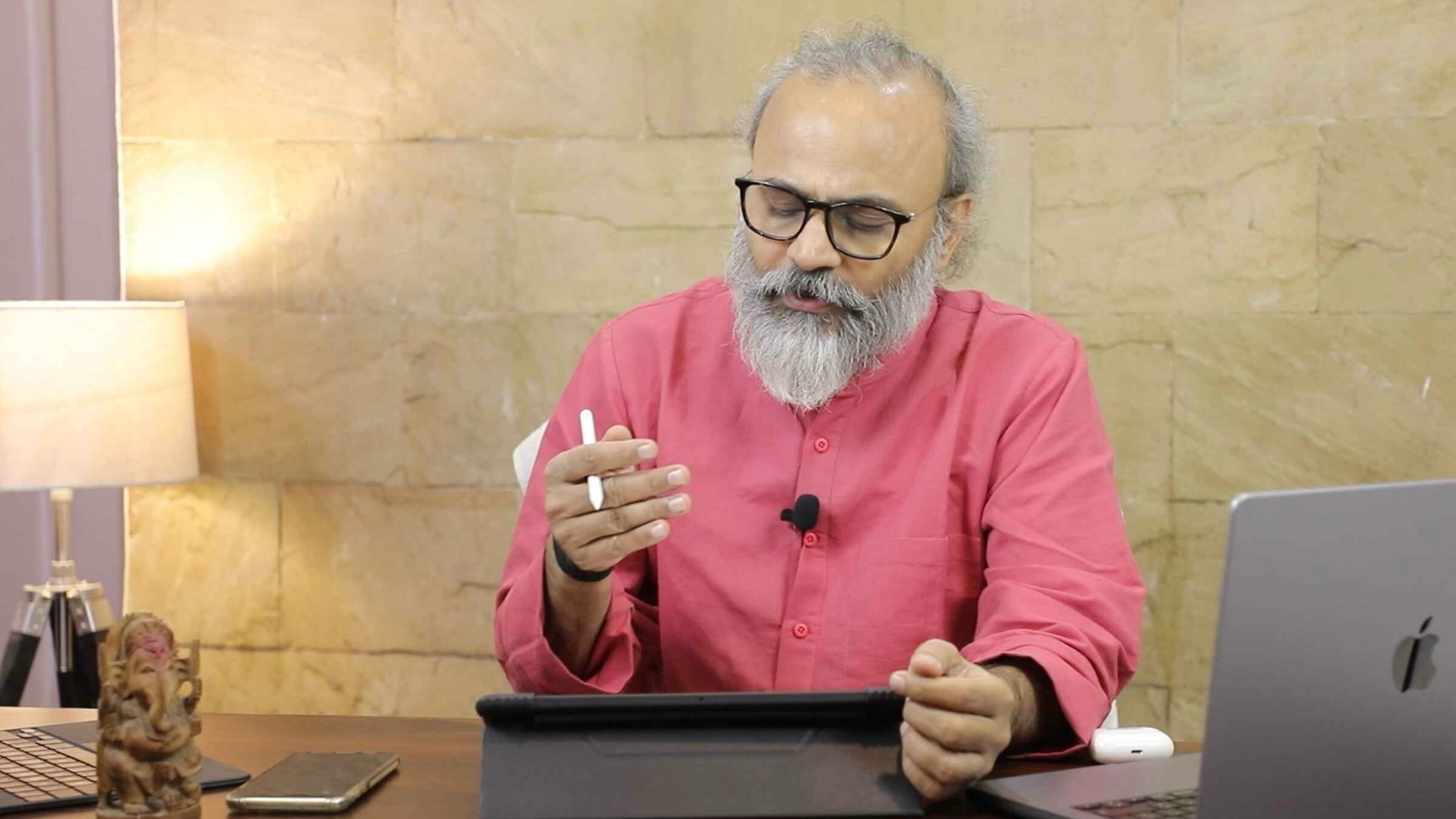
कुंभक: साँसों की गति का ज्ञान
9 months ago By Yogi Anoopकुंभक के अभ्यास के पूर्व सांस की गति को समझना आवश्यक है
गति को बिना समझे गति को स्थिर करना संभव नहीं हो सकता है । मेरे अनुभव में गति में ही ठहराव छिपा हुआ होता है । ज्यादातर स्थिर दिख रही वस्तुओं मे गति छुपी हुई होती है । और गतिमान वस्तु में स्थिरता छुपी हुई होती है । उदाहरण के रूप में इसे समझना आवश्यक है -एक छोटे बच्चे की लंबाई बढ़ रही होती है , किंतु वह गति आँखों से नहीं दिखती है । किंतु गति हो रही होती है । तभी तो बच्चे की लंबाई बढ़ रही होती है । यहाँ तक एक उम्र के बाद भी ऐसा नहीं है कि देह में कोई गति नहीं हो रही होती है । गति मृत्यु पर्यन्त हो रही होती है । इसी गति को समझना होता है । इसी गति में ही स्वाभाविक कुंभक छिपा हुआ होता है । किंतु समान बुद्धि उस स्वाभाविक अल्पविराम को अनुभव नहीं कर पाता है , वह इसलिए क्योंकि उसका ध्यान विराम के उस अल्प क्षण पर न होकर उस तनाव पर होता है जो सामान्यतः दिख रहा होता है ।
जैसे कर्म करते समय मन का तनाव पर होना थकान पैदा करना है, उसे सकाम कर्म कहता हूँ किंतु कर्म के दौरान ही उस पल का अनुभव करते रहना जो थकान के बाद विश्राम का क्षण होता है , उसे मैं निष्काम कर्म कहता हूँ । यह विश्राम का क्षण ही कुंभक व रुकने का क्षण होता है । यह इसलिए क्योंकि रुकने के समय ही विश्राम का अनुभव संभव है । गति में विश्राम संभव नहीं हो सकता है । यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि विषय अर्थात् स्वास के रुकने (कुम्भक) के क्षण में रोकने वाले को अर्थात् कर्ता व आत्मा को स्थिरता का अनुभव होने लगता है । “मैं” स्वयं को परिधि में रखने की अज्ञानता के कारण ही स्वयं को गतिमान समझने की भूल करता है । किंतु जब “मैं” विषय में स्थिरता की अनुभूति करता है तब उसे स्वयं की स्वाभाविक स्थिरता का बोध होने लगता है ।
मैं तो कहता ही हूँ कि जब “मैं” उस परिधि से स्वयं को बाहर करने में समर्थ हो जाता है तब उसे ही निर्वाण कहते हैं । उसी को मैं मुक्ति कहता हूँ । जब तक परिधि में हैं तब तक गतिमान होने का भ्रम बना रहता है , यही भ्रम अज्ञानता है , और यही अज्ञानता दुख है । यही अज्ञानता रोग भी देता है ।
इसीलिए आध्यात्मिक साधना में इसी गति को समझने का प्रयास करते हैं । वाह इसलिए क्योंकि गति को समझे बिना गति की परिधि से मुक्त नहीं हो सकते हैं । इसीलिए स्वयं को केंद्र में स्थापित करने के लिए , यद्यपि यह उसका मूल स्वरूप ही है , कुंभक व विश्राम व स्थिरता का अभ्यास आवश्यक है ।
मेरे अनुभव में कुम्भक को समझने के लिए सबसे पहले पूरक और रेचक अर्थात श्वास को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की गति को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस पूरे कुम्भक वर्कशॉप में मैं चाहता हूँ कि वे लोग ज़्यादा जुड़ें जो हमारा टर्टल योगा या टर्टल ब्रीदिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप या टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर चुके हैं।
उसका कारण यह है कि जब तक आप गति को नहीं समझते, तब तक आप रोकने को नहीं समझ सकते। जब तक आप प्राणायाम को नहीं समझते, तब तक आप होल्ड या कुम्भक को नहीं समझ सकते। उदाहरण देने पर आप इसे समझ पाएँगे।
मान लीजिए आप एक गेंद हवा में फेंकते हैं तो वह ज़ाहिर सी बात है नीचे गिरेगी। वह बहुत तेज़ी से गिरेगी, ज़मीन पर गिरेगी और फिर ऊपर उछलेगी। जब वह ज़मीन पर गिरेगी तो वह तेज़ी से गिरेगी और ज़रा चोट खाएगी ज़मीन से टकराकर, फिर वह वापस ऊपर जाएगी।
अब एक दूसरा उदाहरण लें—यदि मैं एक गेंद को दीवार पर फेंकता हूँ, तो उसे तेज़ गति से मारना बेहतर होता है। अब मैं एक गेंद को हाथ में लेता हूँ और उसे तेज़ी से दीवार पर मारता हूँ, तो वह गेंद दीवार से टकराकर लौटेगी। फिर मैं दोबारा मारता हूँ, वह फिर लौटेगी। यहाँ जो रुकने का समय है, वह बहुत कम होगा।और साथ साथ चोट के लगने की संभावना अधिक भी हो जाती है ।
आप उसे लगातार तेज़ी से दीवार पर मारते हैं और वह वहाँ से टकराकर आती है, और आप उसे फिर से पकड़ते हैं, तो आपको हाथ में भी चोट लगती है । चोट का मतलब यहाँ पर प्रतिक्रिया या प्रभाव से है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुम्भक का होल्डिंग टाइम, चाहे वह गेंद दीवार पर हो या हाथ में, यदि गति तेज़ है तो होल्डिंग टाइम छोटा होगा और उस समय में चोट या प्रतिक्रिया की संभावना अधिक होगी।
इसी प्रकार, यदि मैं इस उदाहरण को प्राणायाम में श्वास पर लागू करूँ और कहूँ कि आप भस्त्रिका करें और उसमें होल्ड करें—क्योंकि भस्त्रिका तेज़ी से की जाती है—तो आप हाथों की मदद से तेज़ी से अंदर सांस लेते हैं, एक सेकंड होल्ड करते हैं, फिर नीचे छोड़ते हैं, फिर एक सेकंड होल्ड करते हैं।
अब आप देखिए कि साँस बहुत तेज़ वॉल्यूम में फेफड़ों में जा रही है और तेज़ी से ही बाहर निकल रही है, इससे फेफड़ों पर बहुत तीव्र झटका पड़ता है और होल्डिंग भी उसी तेज़ गति से हो रही है।
शुरुआत में यदि कोई सामान्य व्यक्ति, बिना किसी निदान के, इस प्रकार के कुम्भक अभ्यास करता है जिसमें गति का कोई नियंत्रण नहीं होता—तो यह बहुत हानिकारक हो सकता है। यह सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं बल्कि मस्तिष्क और हृदय की रक्त-परिसंचरण प्रणाली को भी प्रभावित करता है।
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुम्भक के अभ्यास से पहले श्वास की गति पर नियंत्रण सबसे आवश्यक होता है। अगर आपकी साँस बहुत धीरे-धीरे जा रही है, बहुत धीमी गति से, तो जब वह फेफड़ों में रुकती है तो वहाँ कोई चोट की अनुभूति नहीं होगी।
जैसे आपने गेंद को बहुत तेज़ नहीं, बहुत धीरे छोड़ा हो और वह बस दीवार को छूकर लौट आए। वाह छूने का पल जितना अच्छा और विश्राम देने वाला होता है उतना ही आध्यात्मिक प्रगति होती अहि । यही कुंभक का पल है । उस अवस्था में सिर्फ स्पर्श व विश्राम की अनुभूति ही होती है । वहाँ किसी प्रकार के आघात व चोट की अनुभूति नहीं होती है ।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy