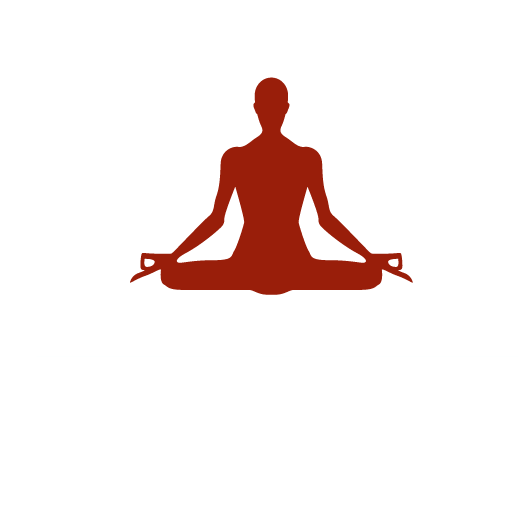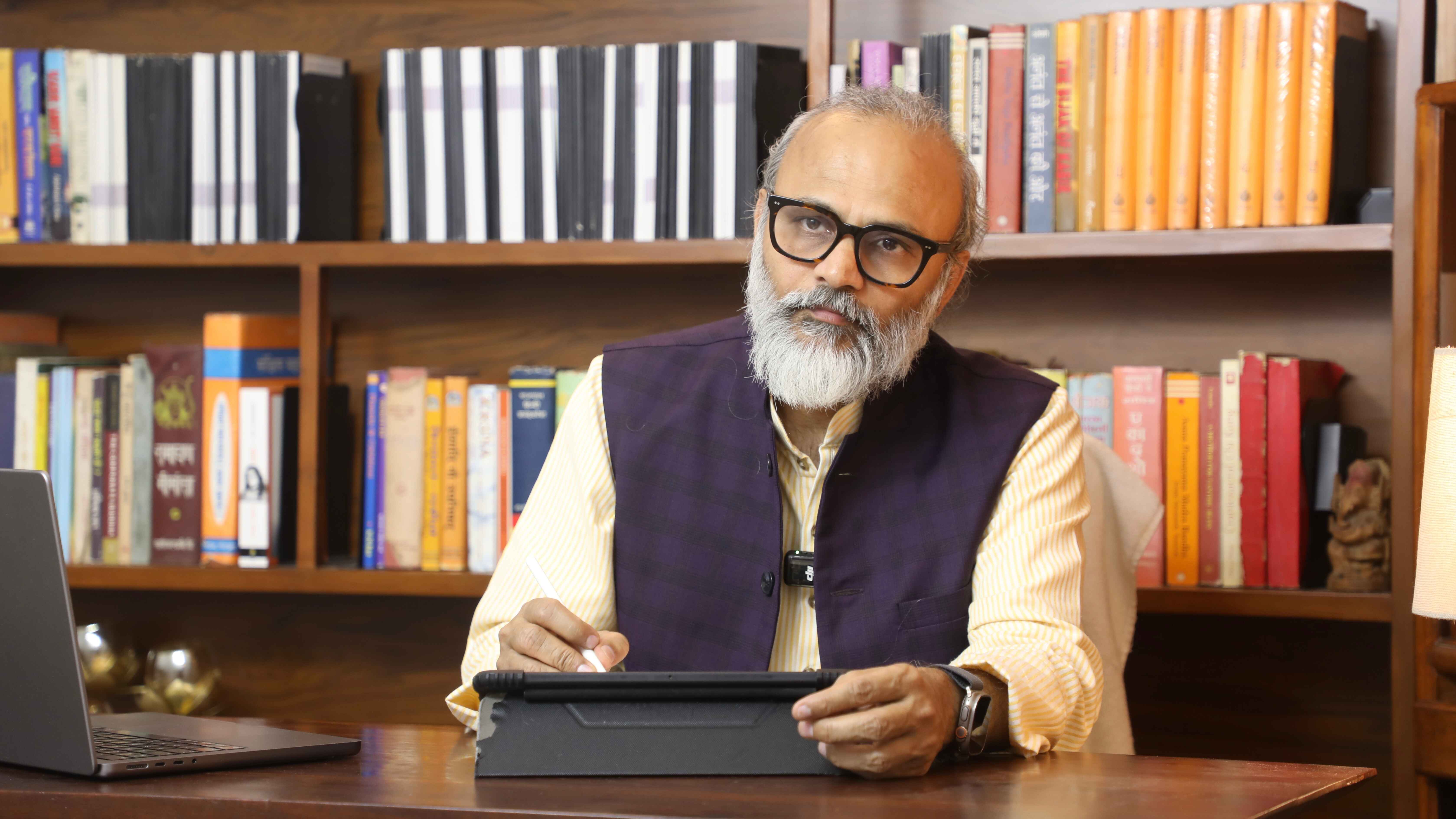
कुंभक क्यों महत्वपूर्ण होता है ?
9 months ago By Yogi Anoopश्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया में कुंभक महत्वपूर्ण होता है
योगी अनूप के द्वारा कुम्भक प्राणायाम के बारे में कहा गया कि जीवन बिना ठहराव के अधूरा है। कुम्भक को भाषा में ठहराव से क्यों जोड़ा जाता है? “मैं विशेष रूप से यह जोड़ता हूँ कि यदि आप कोई भाषा लिखते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं, एक अनुच्छेद लिखते हैं और उस अनुच्छेद में कॉमा और पूर्ण विराम नहीं लगाते, तो लेखक भले ही उसे लिख ले, किंतु जब कोई दूसरा उसे पढ़ेगा, तो वह उससे कुछ समझ नहीं पाएगा।” इसलिए किसी भी भाषा को समझने के लिए अल्पविराम एवं पूर्ण विराम आवश्यक हैं । इसी तरह, जब मैं कुम्भक की बात करता हूँ, तो मैं उसे कुम्भक से जोड़ता हूँ क्योंकि यदि किसी भी भाषा को समझने के लिए अल्पविराम और पूर्ण विराम आवश्यक है, तो उसी तरह श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया में भी कुम्भक आवश्यक है।
कुम्भक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक वाक्य के बाद ठहराव देता है। बिना ठहराव के, बिना श्वास के रुके , न तो कोई अनुपूरक क्रिया संभव है और न ही कोई शुद्धिकरण और साथ साथ न ही कोई समझने की प्रक्रिया । इसलिए यदि शुद्धिकरण से प्रकाश की ओर परिवर्तन हो रहा है, तो वह परिवर्तन तभी संभव है जब बीच में कुम्भक हो। यदि पूरक से रेचन की ओर जाना है, या सामान्य लोगों के लिए कहूँ तो श्वास अंदर लेने के बाद बाहर छोड़ने की प्रक्रिया में जो परिवर्तन आता है, उसमें यह कुम्भक, यह ठहराव, यह अल्पविराम अत्यंत आवश्यक है। बिना रुके पूरक से रेचन या इनहलेशन से एक्सहलेशन की प्रक्रिया हो ही नहीं हो सकती। मैं इसे स्वाभाविक आवश्यक वि प्राकृतिक कुम्भक कहता हूँ । किंतु प्राणायाम के सिद्धों ने कुम्भक इक्षानुसार अभ्यास करने पर बाल दिया , वह इसलिए कि स्वभाव की गहराई को समझ जा सके और गहराई में जाया जा सके ।
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुम्भक में अल्पविराम को गहरे विराम के साथ जोड़ो। यदि आप कोई श्वसन क्रिया कर रहे हैं और उसमें अल्प विराम का अनुभव नहीं हो रहा, यदि आप उस रुकने को महसूस नहीं कर पा रहे, तो आप जो कुछ भी अंदर ले रहे हैं, उसे समझ नहीं पाएँगे और उसकी महत्ता नहीं जान पाएँगे। आप उसे आत्मसात नहीं कर पाएँगे। जैसे आपने एक वाक्य पढ़ा जिसमें कॉमा था, जिसमें पूर्ण विराम था। अब उस पूर्ण विराम का अर्थ यह है कि आपने उस वाक्य को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है, जो आपने पढ़ा था और उसे समझ लिया है। फिर आप अगले वाक्य पर जाते हैं। उसी प्रकार, जब आप श्वास लेते हैं, तो आप श्वास को भीतर लेते हुए अनुभव करते हैं और जब आप उसे रोकते हैं, तो आप कुम्भक की प्रक्रिया करते हैं, जिसे हम अंतर कुम्भक कहते हैं।
जब आप अंतर कुम्भक की प्रक्रिया करते हैं, तो उस कुम्भक के दौरान आपकी स्थिरता, आपकी शांति, आपका एकाग्रता प्रकट होती है, आपकी समझ दिखाई देती है। उस थोड़े से रुकने के क्षण में, उस ठहराव के दौरान, उस श्वसन में स्थिरता की अनुभूति करते हैं । विषय के स्थिर होने पर कर्ता स्वयं को स्थिर अनुभव करता है ।इसीलिए साधना व ध्यान में जब भी किसी चित्र व आकृति पर ध्यान एकाग्र करते हैं तो वह आकृति व चित्र स्थिर होता है । और एकाग्र करने वाला व्यक्ति भी एक स्थान पर स्थिर पूर्वक बैठा हुआ होता है । यदि चित्र चलायमान हो तो स्थिरता की अनुभूति कर पाना साधक के लिए मुश्किल होगा ।
इसी प्रकार साँसों के मध्य उसी रुकने के पल को जिसे कुम्भक कहते हैं , अनुभव करना बहुत आवश्यक होता है । यह अनुभव ही स्थिरता व रुकने का बोध करवाता है । यही बोध ज्ञान देता है । इसी बढ़ती में साँसों की गति को भी समझने का ज्ञान होता है , और साथ साथ स्वयं के स्वभाव को समझने का अनुभव होता है ।
ध्यान दें मेरे अनुभव में कुंभक की ऐक्षिक प्रक्रिया में कभी भी रोकने की अवधि बहुत अधिक नहीं बढ़ानी चाहिए । वह इसीलिए कि कुम्भक का मूल उद्देश्य फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाना नहीं होता है बल्कि शांति और स्थिरता की अनुभूति करना होता है ।
इसी अनुभूति में श्वास को समझने का समय मिलता है ।उसे आत्मसात करने का समय मिलता है । वह चाहे बाहर छोड़ने की प्रक्रिया में कुम्भक हो व अंदर स्स्वास लेने में अंतर्कुम्भक की प्रक्रिया हो । जब आप उसे बाहर रोकते हैं, तो उस कुम्भक की प्रक्रिया को बाह्य कुम्भक कहा जाता है। यह कहा जाता है कि जब आप श्वास को बाहर रोकते हैं, तो आप पूरी प्रक्रिया का अनुभव करते हैं, वही क्षण कुम्भक का होता है। जब आप उसे करते हैं, वही क्षण होता है जब आप अनुभव करते हैं। वह अनुभव का क्षण होता है जब आप अपने मन को विश्राम देते हैं, जब आप अपने आत्म को विश्राम देते हैं। यह भी ध्यान देना उपयुक्त होगा कि जहाँ स्थिरता है , जहाँ भी रुकना है वही पर विश्राम है । वहीं पर समाधि है ।
इसलिए मेरे अनुभव में इस गतिविधि अर्थात् गति के विधि को समझने पर बाल देने के साथ साथ गति के रुकने पर भी बाल देता हूँ । अर्थात् जितनी समझ हो उतना ही कुम्भक का अभ्यास करें, अन्यथा किसी विशेष अनुभवी गुरु केनिर्देशन में रहकर इसका अभ्यास अकड़ें तो बेहतर होगा ।
अंततः कुम्भक करते समय यह समझें कि कुम्भक किसी भयानक अदृश्य ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि मानसिक विश्राम के लिए कर रहे हैं ।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy