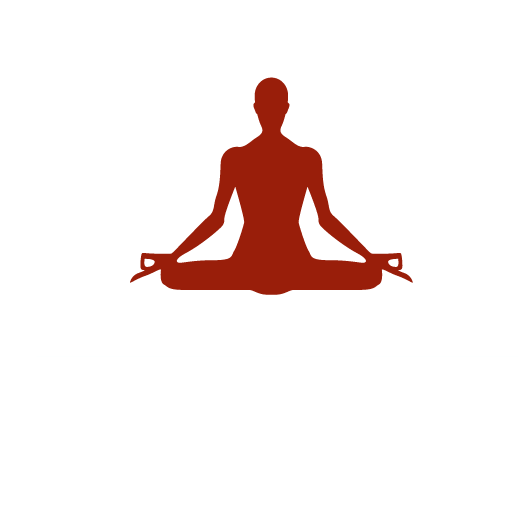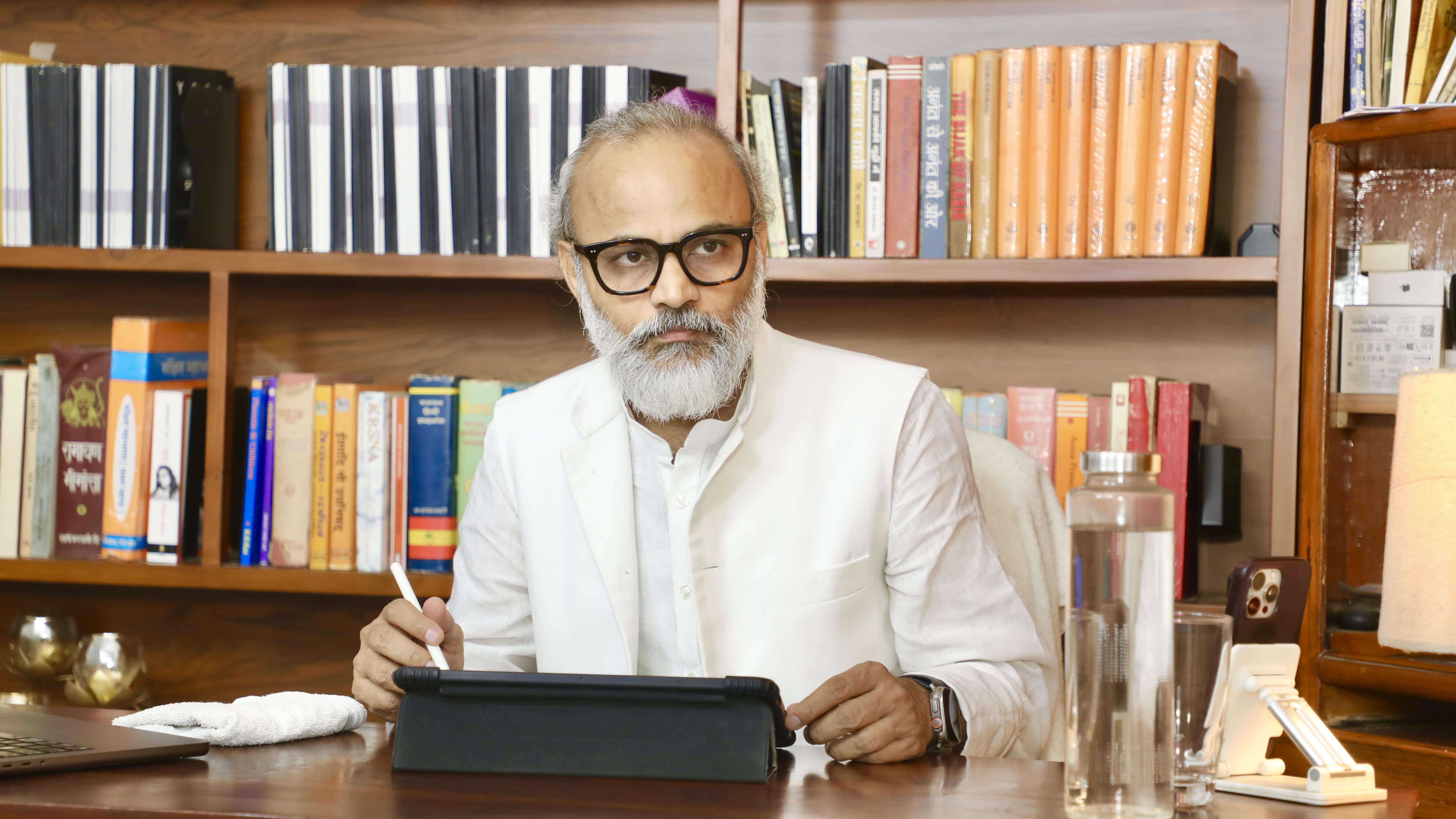
अतिचिंतन: अंतहीन विचार
5 months ago By Yogi Anoopअतिचिंतन: अंतहीन विचार
अतिचिंतन — यह शब्द सुनते ही हमारे सामने मन की वह अवस्था उभर आती है, जब हम किसी एक विचार, समस्या या परिस्थिति को लेकर इतना उलझ जाते हैं कि उससे बाहर निकलने का रास्ता धुंधला पड़ जाता है। पहली नज़र में यह लग सकता है कि गहराई से सोचना एक अच्छी आदत है, क्योंकि इससे समस्याओं के समाधान मिलते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि अतिचिंतन का अधिकांश भाग न तो रचनात्मक होता है और न ही व्यावहारिक। यह केवल विचारों का एक ऐसा जाल है, जिसमें चिंतक स्वयं फँस जाता है।
समस्या का मूल यह है कि चिंतन, स्वभावतः, किसी विषय या दृश्य पर केंद्रित होता है। जब हम किसी बात पर बार-बार सोचते हैं, तो हम उसी सीमित दायरे में घूमते रहते हैं। इस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि विचार पर चिंतन करना ठीक वैसा ही है जैसे आईने में आईने को दिखाना — अंतहीन परावर्तन, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं। एक विचार के तुरंत बाद दूसरा विचार उत्पन्न होता है, फिर तीसरा, और यह सिलसिला चलता ही रहता है। चिंतक को यह आभास तक नहीं होता कि उसका चिंतन व्यावहारिक नहीं है; उसका मन मानो एक पुराने ग्रामोफ़ोन की तरह है जो एक ही धुन पर अटका हुआ है, बस शब्द और चेहरे बदलते रहते हैं।
इस तरह का चिंतन परिणामरहित होता है, क्योंकि यह वास्तविकता से नहीं, बल्कि विचारों की दुनिया से संचालित है। विचार, चाहे कितने भी सुसज्जित क्यों न हों, यदि वे केवल एक-दूसरे का पीछा कर रहे हों, तो वे किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुँचते। वे केवल मन को व्यस्त रखते हैं, और यह व्यस्तता हमें यह भ्रम देती है कि हम किसी गहरी खोज में लगे हैं।
चिंतक के लिए सबसे बड़ा मोड़ तब आता है, जब वह यह समझने लगता है कि वह स्वयं विचार नहीं है, न ही वह कोई दृश्य है जिस पर चिंतन किया जा सके। वह तो चिंतन का स्रोत है — वह बिंदु जहाँ से विचार जन्म लेते हैं। यदि चिंतक स्वयं को एक दृश्य मान लेता है, तो वह अनजाने में अपने ही बनाए विचारों का कैदी बन जाता है। लेकिन जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को देखना शुरू करता है — यह जानना शुरू करता है कि “मैं” किसी विचार या भावना के समान सीमित नहीं हूँ — तब विचारों की यह अंतहीन श्रृंखला टूटने लगती है।
वास्तविक परिवर्तन तब होता है, जब चिंतक ‘स्वयं की अनुभूति’ करने लगता है। यहाँ “स्वयं की अनुभूति” का अर्थ है — उस जागरूकता को पहचानना जो विचारों से परे है, जो विचारों को आते-जाते देख सकती है, लेकिन उनसे बंधी नहीं है। जब यह अनुभूति गहरी होती है, तो मन में एक नया मौन जन्म लेता है। इस मौन में विचार आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन वे हमें बहा नहीं ले जाते। यह वैसा ही है जैसे नदी के किनारे खड़े होकर पानी के बहाव को देखना, बजाय नदी में कूदकर उसमें बहते जाने के।
अतिचिंतन की समस्या का समाधान किसी विचार से नहीं, बल्कि विचार से पीछे हटने से आता है। जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं, बल्कि एक दीपक जलाना होता है — वैसे ही अतिचिंतन को समाप्त करने के लिए विचारों से जूझना नहीं, बल्कि अपने होने की रोशनी को पहचानना होता है।
जब चिंतक इस सरल-सी, किंतु गहरी बात को समझ लेता है कि वह विचारों का विषय नहीं है, बल्कि उनका साक्षी है, तब उसका चिंतन व्यर्थ के चक्र से निकलकर सार्थक दिशा लेने लगता है। और यही वह क्षण है, जब विचारों का जंगल धीरे-धीरे खुलने लगता है, और उसके सामने एक निर्मल आकाश प्रकट होता है — जहाँ मौन है, स्पष्टता है, और एक ऐसी शांति है जो किसी भी समस्या के समाधान से गहरी है।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy