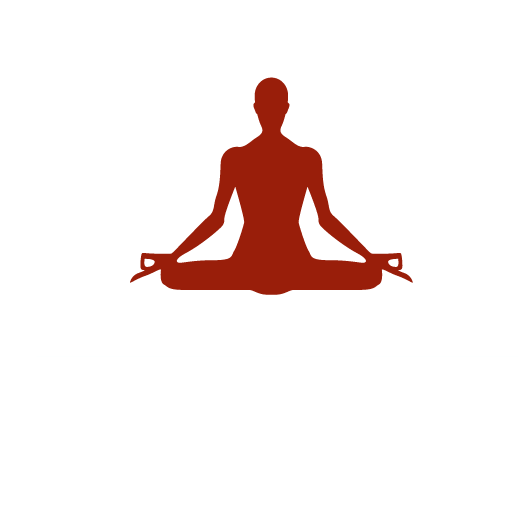आत्म अतिचिंतन: चित्तवृत्ति का अंतहीन प्रवाह
5 months ago By Yogi Anoopआत्म अतिचिंतन: चित्तवृत्ति का अंतहीन प्रवाह
योगिक दृष्टि से मन का स्वभाव है — चित्तवृत्ति अर्थात विचारों और भावनाओं का सतत प्रवाह। पतंजलि योगसूत्र के पहले ही सूत्र में कहा गया है — योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योग वह अवस्था है जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यहाँ “वृत्ति” का अर्थ केवल बाहरी चिंतन नहीं, बल्कि वह आंतरिक गतिविधि भी है जो विचार, कल्पना, स्मृति और स्वप्न के रूप में लगातार चलती रहती है।
अतिचिंतन इसी वृत्ति का एक विकृत रूप है। यह वह अवस्था है जिसमें चिंतक (मैं) किसी अंततः कारण में स्वयं को ही विषय मानकर इस हद तक चिंतन में उलझ जाता है कि उसका सारा ध्यान केवल विचारों के अंतहीन अनुक्रम में फँसा रहता है। उसे यह लग सकता है कि वह स्वयं के बारे में चिंतन कर रहा है परंतु वास्तविकता में उसका यह चिंतन स्वयं को विषय मानकर ही एक वृत्ताकार पथ पर चल रहा होता है — जहाँ प्रारंभ और अंत में कोई भेद नहीं। जहाँ पर विषय , आत्मा के रूप में प्रतीत होता है ।
मैं कहता है कि जब चिंतन का केंद्र विषय (Object) या दृश्य (Seen) पर हो, तो वह चिंतन कभी भी अंत तक नहीं पहुँच सकता। कारण यह है कि वह विषय या दृश्य स्वयं के द्वारा ही निर्मित हैं । यहाँ पर चिंतक ही स्वयं को विषय मानकर चिंतन कर रहा होता है । इस चिंतन का अंत संभव ही नहीं हो सकता है । क्योंकि यहाँ सब कुछ माना जा रहा है । और जब भी मानकर कोई क्रिया की जाती है उसके परिणाम का अंत संभव नहीं है ।
यह कुछ ऐसे ही होगा जैसे — रेत की मुट्ठी को कसकर पकड़ना। जितना कसोगे, उतनी ही जल्दी वह हाथ से फिसलेगी। एक विचार के पीछे दूसरा विचार उत्पन्न होता है, फिर तीसरा, और यह शृंखला बिना रुके चलती रहती है। यह सब इसलिए हो रहा है कि आप को पूर्ण ज्ञात ही नहीं है ।
चिंतक की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अज्ञानवश स्वयं को “विषय व विचार” के स्तर पर परिभाषित करने लगता है। वह यह भूल जाता है कि वह न तो विचार है और न ही विचार का विषय, बल्कि वह विषय का निर्माता है । जिस पल उसे यह बोध होता है कि उसने ही स्वयं को विषय बनाया हुआ है , उसी पल वह विषय छोड़ देता है । यही पल स्व-बोध का है ।
इस पल तो उसे द्रष्टापन (Witness) की भी अनुभूति नहीं हो सकती है क्योंकि क्योंकि उसने दृश्य निर्मित करना बंद कर दिया है । उसने उन सभी साधनों (इन्द्रियों , मस्तिष्क एवं मन) से भी विषय निर्माण के लिए सहायता लेना बंद का दिया होता है । कहने का मूल अर्थ है , कि उस “मैं” को यह बोध हो चुका हुआ होता है वह मूलतः शुद्धतः चेतन है ।
जब तक चिंतक यह नहीं समझता कि वह स्वयं को ही चिंतन के विषय के रूप में बना लेता है तब तक उसे बोध नहीं हो सकता है । वह चिंतन जैसी क्रिया से मुक्त नहीं हो सकता है । अज्ञानतावश इस प्रकार की वैचारिक क्रिया को ही मैं अतिचिंतन कहता हूँ जो जो पांचों विषय से कहीं परे है ।
ध्यान की साधना में यह बोध ज्ञानी अनुभवी गुरु से वार्तालाप से ही सबसे अधिक प्राप्त हो सकती है । वार्तालाप से और उसके बाद ध्यान अभ्यास से संभव है । मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किताबों के माध्यम से भी इस प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है । वह इसलिए कि किताबों वह माध्यम है जो सिर्फ़ एक ही तरफ़ से ज्ञान दे रही होती है , उसको जिस तरह आप समझते हो उसी तरह आप क्रिया करोगे । आपके समझने का दृष्टिकोण यदि अल्पतर है तो आप उसे समझ ही नहीं सकते हो । और यदि आप उस पुस्तक से कहीं अधिक अच्छा दृष्टिकोण रखते हो तो आप भ्रमित हो सकते हो ।
इसलिए सबसे पहले एक ऐसा गुरु होना चाहिए जिससे आपका सीधा संवाद हो सके । जब भी आप सशंकित हों , तब आप उससे अपने भ्रम के निवारण के लिए समाधान ले सकें । और तब आप जैसे-जैसे यह ठहराव बढ़ता है, चिंतन की अनावश्यक परतें अपने आप गिरने लगती हैं।
जब यह बोध पक्का हो जाता है, तो चित्तवृत्ति स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है। तब मन के भीतर एक मौन और स्पष्टता जन्म लेती है, जो किसी समाधान का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे अपने होने का स्वभाव है। यही वह अवस्था है जहाँ अतिचिंतन समाप्त होता है, और आत्मदर्शन का द्वार खुलता है — वही द्वार जिसे योग ने सदियों से कैवल्य के नाम से जाना है।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy